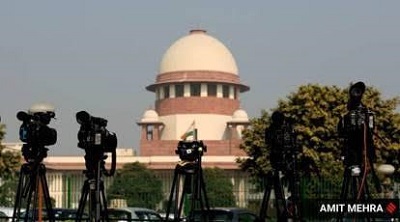संदर्भ
वर्तमान समय में न्यायिक समीक्षा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) और इससे संबंधित नियमों की संवैधानिकता पर महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रहा है। इन नियमों की अस्पष्टता से उत्पन्न चिंताओं के कारण इनके निवारण की आवश्यकता और बढ़ गई हैं, विशेषकर उन आवेदकों के मामले में जिनके नागरिकता संबंधी अनुरोधों को अस्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त, बिना अपनी मूल नागरिकता का त्याग किए विदेशी आवेदकों के लिए दोहरी नागरिकता की चिंताओं ने इस कानून के साथ के विपरीत स्थिति को पैदा किया है।
न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता
संविधानिक न्यायालयों के द्वारा कानूनों को अवैध घोषित करना एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। सामान्यतः, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को तब तक वैध माना जाता है जब तक वे स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते। इस सिद्धांत को मनीष कुमार बनाम भारत संघ (2021) में देखा गया गया था, इसमे कहा गया था कि विधायी प्रक्रियाएं द्वेष से मुक्त होती हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुदेवदत्ता वीकेएसएसएस मर्यादित और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2001) मामले कहा था कि "विधायी दुर्भावना कानून न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से परे होते है"।
हालांकि, यह पारंपरिक निर्णय आधुनिक चुनौतियों का समाधान करने में अपर्याप्त है, जो प्रायः लोकलुभावन सरकारों द्वारा प्रेरित हैं या लक्षित कानूनों का निर्माण कर रहीं हैं। ऐसी सरकारें विधान प्रक्रियाओं के माध्यम से चुनावी प्रणाली में भी हेरफेर कर सकती हैं। यह आधुनिक प्रवृत्ति एक अधिक उन्नत और सशक्त न्यायिक दृष्टिकोण की मांग करती है। बिना किसी मंशा की जांच किए कानूनों की वैधता के बारे में पुरानी धारणाओं का पालन करना संवैधानिक न्यायालयों की भूमिका को कमजोर कर सकता है।
विधायी प्रक्रिया की राजनीतिक प्रकृति
विधायिका स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक संस्थान है। ऐसी सरकारें जो संवैधानिक लोकतंत्र की उपेक्षा करती हैं, वे संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत कानून बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। ऐसी स्थितियों में, कानूनों की वैधता के विषय में न्यायिक उत्साह (judicial euphoria) ने कई बार सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने से रोका है। विमुद्रीकरण के दौरान विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ (2023) मामले में स्थगन आदेश जारी न करने के निर्णय ने अपरिवर्तनीय परिणामों को पैदा किया। इसी प्रकार, अनुच्छेद 370 के मामले में कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के संबंध में गैर-हस्तक्षेप ने संबंधित मुकदमे को लगभग अप्रासंगिक बना दिया।
इसके विपरीत, अनुप बरणवाल बनाम भारत संघ (2023) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक क्रांतिकारी निर्णय दिया था, इस निर्णय में बिना कार्यकारी प्रभुत्व के चुनाव आयोग के चयन के लिए एक स्वतंत्र निकाय का समर्थन किया गया था। हालांकि इसके बावजूद, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति को चयन करने की शक्ति प्रदान की, जो कि पुरानी प्रणाली ही है। इस अधिनियम को, जया ठाकुर बनाम भारत संघ (2024) मामले में अनुमति प्रदान की गई, इस तथ्य के बावजूद कि यह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लोकतांत्रिक आधार को खतरे में डालता है।
लक्षित कानून और इसके प्रभाव
सीएए और इससे संबंधित नियम लक्षित कानून के स्पष्ट उदाहरण हैं, जहाँ विधायी दुर्भावना स्पष्ट दिखाई देती है। यह कानून नागरिकता प्रक्रिया से मुसलमानों को धर्म के आधार पर बाहर करता है। इसी तरह, शायरा बानो (2017) मामले में ट्रिपल तलाक कानून की अवैधता के बावजूद, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम (2019) ने तत्काल तीन तलाक को अपराध घोषित किया। इस कानून का लक्ष्य मुस्लिम समुदाय था, जो प्रायः मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल रहा । हालांकि इसके बजाय कानून से संबंधित विभाजनकारी एजेंडा को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा कुछ राज्यों में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून लक्षित कानूनों का अन्य उदाहरण हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका में, पारंपरिक विचारों के लोगों के समूह के द्वारा भी दुर्भावना के आधार पर कानूनों के न्यायपालिका द्वारा निरस्तीकरण का विरोध किया गया। कानूनी विद्वान जॉन हार्ट एली ने राजनीतिक संथाओं की कथित बुरी मंशाओं को दंडित करने के लिए संविधान का उपयोग करने के खिलाफ तर्क दिया। हालांकि, प्रेरित कानूनों की, जो भेदभावपूर्ण इरादों को दर्शाते हैं, कठोर न्यायिक जांच की जानी चाहिए। जैसा कि सुज़ाना डब्ल्यू. पॉलवोग्ट ने कहा है कि , "द्वेष कभी भी समान सुरक्षा विश्लेषण के उद्देश्यों के लिए वैध राज्य हित नहीं हो सकता।" संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का संयुक्त राज्य कृषि विभाग बनाम मोरेनो (1973) मामले मे निर्णय में "हिप्पियों" को सामूहिक आवासीय अधिकारों से बाहर करने वाले कानून को निरस्त कर दिया था, इस निर्णय ने स्पष्ट किया था कि ऐसे बहिष्कारपूर्ण कानून भेदभावपूर्ण इरादे का संकेत देता है।
भारतीय न्यायिक उदाहरण
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में प्रभावी रूप से संसदीय कानूनों के संचालन को रोक दिया है। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2007) मामले में, पेशेवर कॉलेजों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उम्मीदवारों के लिए 27% कोटा के संबंध में, न्यायालय ने एक निषेधाज्ञा जारी की थी। इसी तरह, राकेश वैष्णव बनाम भारत संघ (2021) में, न्यायालय ने विवादास्पद कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया था, जिसे केंद्र ने अंततः किसानों के व्यापक विरोध के बाद वापस ले लिया था।
उन कानूनों के लिए जो स्पष्ट रूप से असंवैधानिक या विभाजनकारी हैं, न्यायिक समीक्षा मजबूत, तत्काल और स्पष्ट होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को अपने पिछले कार्यों से सीखना चाहिए और महत्वपूर्ण समय के दौरान अपनी संवेदनहीनता के राजनीतिक परिणामों को समझना चाहिए। विलंब अक्सर संवैधानिक निर्णय के उद्देश्य को विफल कर देता है, जिससे दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक कानूनों के समाधान के लिए समय पर न्यायिक समीक्षा आवश्यक हो जाती है।
निष्कर्ष
निष्कर्षतः, न्यायपालिका को समकालीन चुनौतियों के अनुकूल होना चाहिए और कानूनों की समीक्षा में एक अधिक आक्रामक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कानूनों की वैधता का मतलब उन कानूनों को कठोर जांच से बचाना नहीं है जो स्पष्ट रूप से प्रेरित या लक्षित हैं। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा में अपनी भूमिका को पूरा कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कानून संविधान में निहित सिद्धांतों को दर्शाते हैं न कि लोकलुभावन सरकारों की इच्छाओं को। महत्वपूर्ण समयों में, सभी नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मजबूत न्यायिक निर्णय अनिवार्य है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखता है।
|
यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न
|
स्रोत: द हिन्दू