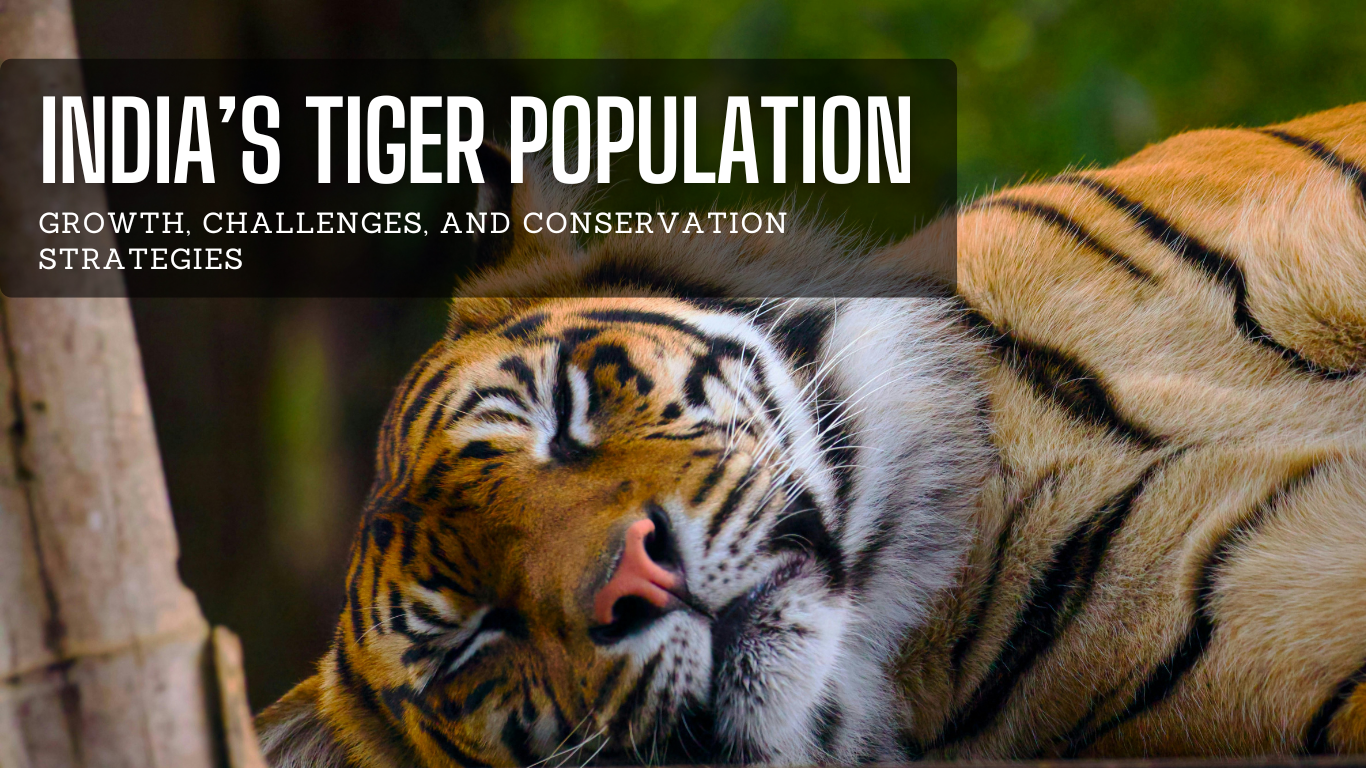सन्दर्भ : भारत, दुनिया के लगभग 75% बाघों का घर है और यहाँ बाघों की आबादी में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जो बाघ संरक्षण पहलों की सफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार, वर्तमान जनसंख्या 3,682 (रेंज: 3,167-3,925) है, जो 2018 में 2,967 और 2014 में 2,226 से उल्लेखनीय वृद्धि है। लगातार सैंपल किए गए क्षेत्रों में 6% वार्षिक वृद्धि दर के साथ, यह वृद्धि बाघ संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। हालांकि, यह प्रगति आवास की हानि, मानव-वन्यजीव संघर्ष और सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों जैसी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करती है, जो बाघों के अस्तित्व को प्रभावित करना जारी रखती हैं।
संरक्षण रणनीतियाँ और सरकारी पहल:
भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्रबंधित करने और बाघ संरक्षण को समर्थन देने के लिए तीन-आयामी रणनीति अपनाई है:
1. सामग्री और रसद सहायता: प्रोजेक्ट टाइगर की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से, बुनियादी ढांचे के विकास, संघर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए रिजर्व को धन मुहैया कराया जाता है। वित्तीय सहायता जागरूकता अभियान, स्थिरीकरण उपकरण और ट्रैंक्विलाइज़र सहित अन्य उपकरणों की खरीद के लिए प्रदान की जाती है।
2. आवास हस्तक्षेप को सीमित करना: संरक्षण प्रयास रिजर्व के भीतर बाघों की आबादी को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि कोई रिजर्व अपनी वहन क्षमता तक पहुँच जाता है, तो अत्यधिक वन्यजीव फैलाव को रोकने के लिए हस्तक्षेप को सीमित कर दिया जाता है, जिससे मानव-पशु संघर्ष में कमी आती है। बफर ज़ोन में आवास संशोधनों पर नियंत्रण रखा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाघ स्वाभाविक रूप से अन्य समृद्ध वन क्षेत्रों में फैल सकें।
3. मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी): एनटीसीए ने संघर्ष स्थितियों के प्रबंधन के लिए तीन एसओपी जारी किए हैं:
o मानव-बहुल क्षेत्रों में बाघों का भटकना
o पशुओं पर बाघ के हमले
o बाघों को उनके मूल क्षेत्रों से कम आबादी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करना
यह एसओपी बाघों की संख्या में हो रहे विस्तार को नियंत्रित करने, पशुधन से संबंधित संघर्षों को रोकने और विभिन्न परिदृश्यों में जनसंख्या संतुलन सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त, बाघ संरक्षण योजनाओं (टीसीपी) के तहत, परियोजना बाघ निधि द्वारा समर्थित, साइट-विशिष्ट हस्तक्षेप किए जाते हैं।
बाघों की संख्या और आवास विस्तार:
साइंस में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में पिछले दो दशकों में 138,200 वर्ग किलोमीटर में बाघों की संख्या में 30% की वृद्धि देखी गई है, जबकि 35,255 वर्ग किलोमीटर में फैले संरक्षित क्षेत्रों (पीए) में बाघों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई है। बाघों के प्रमुख आवास के रूप में काम करने वाले इन क्षेत्रों के अलावा, बाघ अब लगभग 60 मिलियन लोगों के निवास वाले क्षेत्रों में भी चले गए हैं।
अध्ययन में 2006 से 2018 तक 20 भारतीय राज्यों में बाघों की संख्या में वृद्धि का विश्लेषण किया गया, जिसमें परिदृश्यों को 10x10 किमी के ग्रिड में विभाजित किया गया। निष्कर्षों से बाघों के आवासों में क्रमिक विस्तार का पता चलता है:
● 2006-2010: 35% नए क्षेत्रों का विस्तार हुआ
● 2010-2014: 20% नए क्षेत्रों का विस्तार हुआ
● 2014-2018: 45% नए क्षेत्रों का विस्तार हुआ:
बाघ उच्च शिकार घनत्व, कम मानवीय गतिविधि और मध्यम आर्थिक समृद्धि वाले आवासों को पसंद करते हैं। उनका अधिभोग शिकार प्रजातियों जैसे चित्तीदार हिरण (एक्सिस एक्सिस), सांभर हिरण (रुसा यूनिकोलर), दलदली हिरण (रुसर्वस डुवाउसेली), और गौर (बोस गौरस) के वितरण से निकटता से जुड़ा हुआ है। ये शाकाहारी जानवर बाघों की उपस्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, बाघ के आवास अन्य बड़े मांसाहारी और विशाल जीवों के साथ भी फैले हुए हैं:
● एशियाई हाथी (59%)
● गौर (84%)
● तेंदुए (62%)
● ढोल (68%)
● सुस्त भालू (51%)
यह अम्ब्रेला प्रजाति अवधारणा को मजबूत करता है, जहाँ बाघ संरक्षण अप्रत्यक्ष रूप से जैव विविधता को संरक्षित करके और कार्बन पृथक्करण में योगदान देकर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ पहुँचाता है—जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में एक महत्वपूर्ण कारक है।
स्थानीय बाघ विलुप्ति और संरक्षण चुनौतियां:
सकारात्मक वृद्धि के बावजूद, 12 वर्षों में 17,992 वर्ग किमी में स्थानीय विलुप्तियाँ दर्ज की गई हैं, जिनमें सबसे अधिक हानि निम्नलिखित के बीच हुई है:
o 2006-2010: कुल स्थानीय विलुप्तियों का 64%
o 2010-2014: 17%
o 2014-2018: 19%
सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र पूर्वी भारत, विशेषकर छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में हैं, जहां निम्नलिखित रिज़र्व हैं:
o गुरु घासीदास
o पलामू
o उदंती-सीतानदी
o सिमलीपाल
o इंद्रावती
यह क्षेत्र गंभीर संरक्षण खतरे से गुजर रहे हैं। भारत के सबसे गरीब जिलों में से ये क्षेत्र बुशमीट शिकार, अवैध शिकार और आवास क्षरण से पीड़ित हैं, जिससे बाघों का पनपना मुश्किल हो रहा है।
बाघ संरक्षण पर सशस्त्र संघर्ष का प्रभाव:
सबसे चौंकाने वाले अध्ययनों में से एक यह है कि सशस्त्र संघर्ष और बाघों के विलुप्त होने के बीच सीधा संबंध है। लगभग 47% बाघों की विलुप्ति नक्सली विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में दर्ज की गई, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ (इंद्रावती, अचानकमार, उदंती-सीतानदी) और झारखंड (पलामू) में। नागार्जुनसागर-श्रीशैलम, अमराबाद और सिमिलिपाल जैसे क्षेत्रों में, जहाँ सशस्त्र संघर्ष कम हो गया है, वहाँ बाघों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। फिर भी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सशस्त्र विद्रोह संरक्षण प्रयासों में बाधा डाल रहे हैं, जिससे वन्यजीव संरक्षण के लिए एक अस्थिर वातावरण उत्पन्न हो रहा है।
मानव-बाघ सह-अस्तित्व: सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और कर्नाटक जैसे कुछ घनी आबादी वाले राज्यों में बाघ पनपते हैं, जहाँ संरक्षण प्रयासों को निम्नलिखित द्वारा समर्थन दिया जाता है:
o पारिस्थितिकी पर्यटन राजस्व
o सरकारी मुआवज़ा योजनाएँ
o समुदाय-आधारित संरक्षण परियोजनाएँ
इन क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया गया है तथा स्थानीय लोग बाघ-संबंधी पर्यटन और संरक्षण पहलों से लाभान्वित हुए हैं।
इसके विपरीत, उच्च गरीबी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बाघों के बसने की दर सबसे कम है, जहाँ समुदाय आजीविका के लिए जंगलों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। वैकल्पिक आय स्रोतों और उचित जागरूकता की कमी इन क्षेत्रों में संरक्षण प्रयासों को मुश्किल बनाती है।
स्थिरता और भविष्य की संरक्षण रणनीतियाँ:
अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि आर्थिक समृद्धि दोहरी भूमिका निभाती है—जहाँ टिकाऊ पारिस्थितिकी पर्यटन और संरक्षण निधियाँ बाघों की संख्या में वृद्धि करती हैं, वहीं अत्यधिक शहरीकरण और भूमि-उपयोग परिवर्तन बाघों के आवासों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
पारिस्थितिकी विकास परियोजनाओं में निवेश और सामुदायिक भागीदारी टिकाऊ संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। संरक्षित क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण, गरीबी उन्मूलन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मॉडल के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे स्थानीय समुदायों को संरक्षण की सफलता से लाभ मिल सके।
साथ ही, अवैध शिकार, आवास विनाश और अतिक्रमण से निपटने के लिए वन्यजीव कानूनों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। विधायी उपाय जैसे:
o भूमि संरक्षण नीतिया
o वन भूमि के परिवर्तन पर प्रतिबंध
o सतत विकास योजना
बाघों की आबादी की सुरक्षा के लिए इस कानून को बरकरार रखा जाना चाहिए।
निष्कर्ष:
भारत के बाघ संरक्षण प्रयास वैश्विक सफलता की उदाहरण पेश करते हैं, जिसमें कानूनी ढांचा, वैज्ञानिक निगरानी और सरकारी हस्तक्षेप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, आवास विखंडन, मानव-वन्यजीव संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं की चुनौतियों पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है।"
भविष्य की रणनीतियों पर ध्यान केन्द्रित होना चाहिए:
● आर्थिक विकास के साथ संरक्षण को संतुलित करना।
● सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना।
● अवैध शिकार विरोधी प्रयासों को मजबूत करना।
● टिकाऊ भूमि उपयोग प्रथाओं को सुनिश्चित करना।
समग्र और समावेशी दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए, भारत बाघ संरक्षण में विश्व का नेतृत्व करना जारी रख सकता है और एक ऐसा भविष्य सुनिश्चित कर सकता है जहाँ बाघ और मानव सौहार्दपूर्ण ढंग से सह-अस्तित्व में रह सकें।
|
मुख्य प्रश्न: भारत में बाघों की संख्या और स्थानीय विलुप्ति को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों, जैसे गरीबी, सशस्त्र संघर्ष और भूमि-उपयोग परिवर्तन की भूमिका पर चर्चा करें। अपने तर्कों का समर्थन उदाहरणों से करें। |