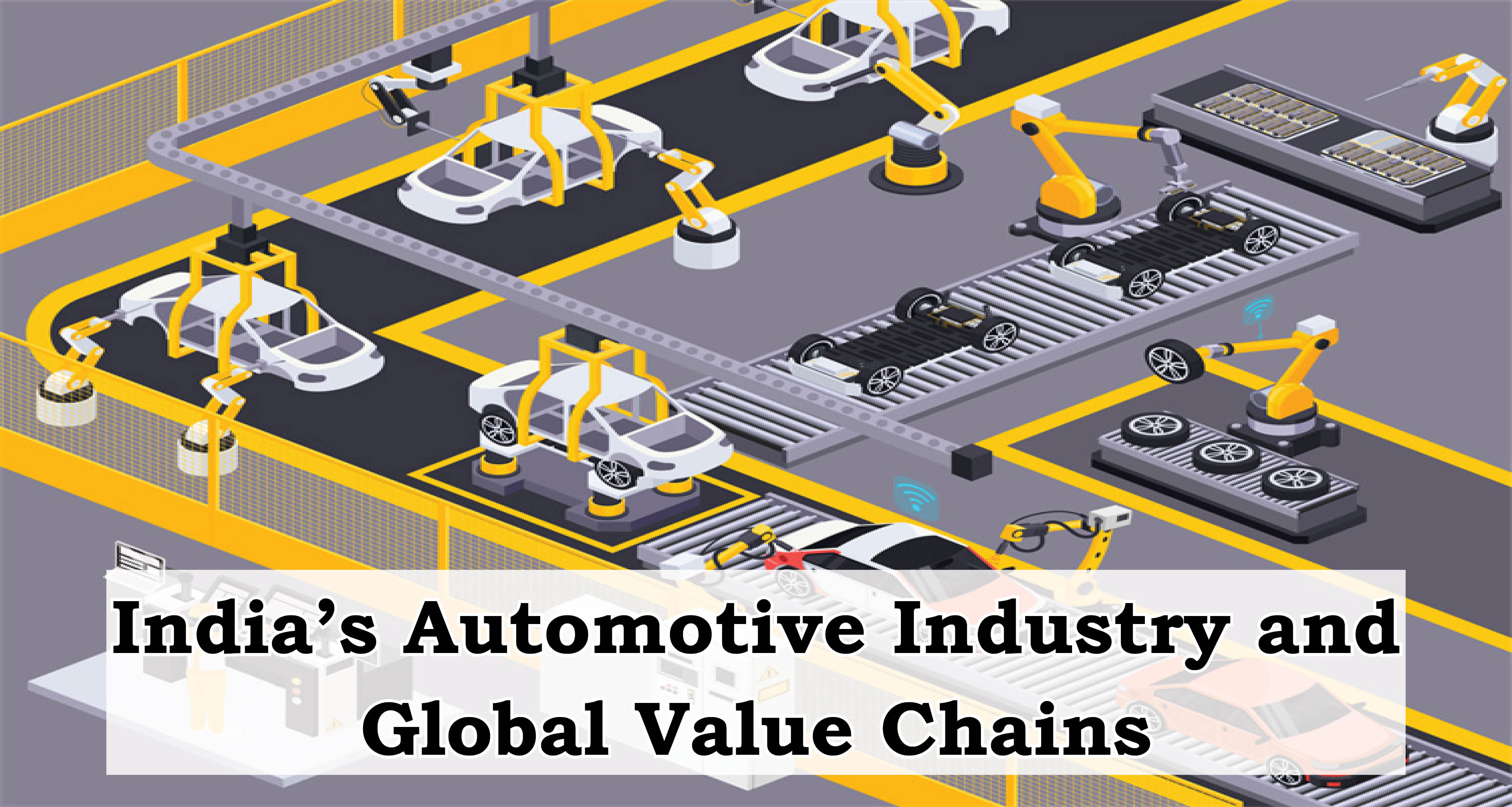नीति आयोग ने हाल ही में "ऑटोमोटिव इंडस्ट्री: पावरिंग इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन" नामक एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देश के ऑटोमोबाइल क्षेत्र का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में भारत की वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ, और वैश्विक ऑटोमोबाइल प्रणाली में भारत की भागीदारी को बढ़ाने की रणनीति प्रस्तुत की गई है।
वैश्विक और घरेलू ऑटोमोबाइल परिदृश्य में भारत की वर्तमान स्थिति
- 2023 तक, वैश्विक ऑटोमोबाइल उत्पादन लगभग 94 मिलियन यूनिट्स था। वैश्विक स्तर पर ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का बाजार लगभग 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें से लगभग 700 अरब डॉलर का हिस्सा निर्यात का था। इस परिदृश्य में, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक बन चुका है, केवल चीन, अमेरिका और जापान से पीछे, और भारत का घरेलू उत्पादन हर साल लगभग 6 मिलियन वाहनों तक पहुँच गया है।
- भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में उल्लेखनीय उपस्थिति रखता है। भारत की प्रमुख ताकत छोटे वाहनों और यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में है। 'मेक इन इंडिया' जैसी सरकारी पहलों और लागत-कुशल श्रमशक्ति के कारण भारत ने ऑटोमोबाइल निर्माण और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनने की ओर मजबूत कदम बढ़ाया है।
वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में परिवर्तनकारी प्रवृत्तियाँ
- वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग एक बड़े परिवर्तन से गुजर रहा है, जिसका मुख्य कारण इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की ओर बदलाव है। यह बदलाव टिकाऊ परिवहन की उपभोक्ता मांग, पर्यावरणीय नियमों में वृद्धि और बैटरी तकनीक में तेजी से हो रहे नवाचारों से प्रेरित है। ईवी अपनाने में तेजी पारंपरिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बदल रही है और लिथियम व कोबाल्ट जैसी खनिजों में निवेश को बढ़ावा दे रही है, जो बैटरी निर्माण के लिए आवश्यक हैं।
- ईवी क्रांति के समानांतर, इंडस्ट्री 4.0 का उदय ऑटोमोबाइल निर्माण प्रक्रियाओं को नया रूप दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने, संचालन लागत घटाने और लचीलापन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये डिजिटल नवाचार स्मार्ट फैक्ट्रियों और कनेक्टेड वाहनों की नींव रख रहे हैं और ऑटोमोबाइल निर्माण के दायरे को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं।
भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बाधाएँ
हालाँकि भारत वाहन निर्माण में अग्रणी है, लेकिन वैश्विक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 3% है, जो लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर है। उच्च-प्रेसिजन सेगमेंट जैसे इंजन कंपोनेंट्स, ड्राइव ट्रांसमिशन, और स्टीयरिंग सिस्टम में भारत की भागीदारी केवल 2-4% तक सीमित है, जबकि ये क्षेत्र वैश्विक व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
कई चुनौतियाँ भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) में गहरी भागीदारी से रोकती हैं, जिनमें शामिल हैं:
• उच्च परिचालन लागत
• अपर्याप्त बुनियादी ढांचा
• अनुसंधान एवं विकास (R&D) में कम निवेश
• वैश्विक स्तर पर सीमित एकीकरण
• उन्नत विनिर्माण क्षमताओं पर अपर्याप्त ध्यान
रणनीतिक रोडमैप और प्रस्तावित हस्तक्षेप
इन समस्याओं से निपटने के लिए, नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने हेतु कई वित्तीय और गैर-वित्तीय उपायों की सिफारिश की गई है। ये रणनीतियाँ ऑटोमोबाइल पुर्जों की जटिलता और परिपक्वता के स्तर के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं- इमर्जिंग और कॉम्प्लेक्स, कन्वेंशनल और कॉम्प्लेक्स, कन्वेंशनल और सिंपल, इमर्जिंग और सिंपल।
वित्तीय हस्तक्षेप
इनमें शामिल हैं:
• ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर (Opex) सपोर्ट: निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन, विशेष रूप से टूलिंग, डाई और सहायक बुनियादी ढाँचे में पूंजीगत व्यय (Capex) पर ध्यान।
• कौशल विकास: एक कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए समर्पित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, जिससे दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके।
• R&D और ब्रांडिंग सपोर्ट: अनुसंधान और नवाचार को सरकारी प्रोत्साहनों के माध्यम से बढ़ावा देना, साथ ही MSMEs को सशक्त बनाने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) ट्रांसफर की सुविधा। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों के अलग पहचान हेतु ब्रांडिंग पर भी ज़ोर।
• क्लस्टर विकास: विभिन्न कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने हेतु साझा सुविधाओं जैसे R&D सेंटर, टेस्टिंग लैब और सप्लाई चेन समर्थन इकाइयों की स्थापना।
गैर-वित्तीय हस्तक्षेप
रिपोर्ट में सुझाए गए प्रमुख गैर-आर्थिक उपायों में शामिल हैं:
• इंडस्ट्री 4.0 तकनीकों को बढ़ावा: स्मार्ट निर्माण प्रणालियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना जो दक्षता बढ़ाएं, लागत कम करें और टिकाऊ विकास को समर्थन दें।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग: संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करना और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTA) के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुँच बनाना।
• नियामकीय सुधार और व्यापार सुगमता: नीतियों को सरल बनाना, श्रम नियमों में लचीलापन लाना, सप्लायर से कनेक्शन बेहतर बनाना, और ऑटोमोबाइल कंपनियों के संचालन को आसान बनाना।
2030 की दृष्टि: वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ते कदम
नीति आयोग ने 2030 तक भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक महत्वाकांक्षी और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जो प्रस्तावित उपायों के सफल कार्यान्वयन पर आधारित है। रिपोर्ट में निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं:
• ऑटोमोटिव कंपोनेंट उत्पादन: 2030 तक उत्पादन को 145 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना।
• निर्यात में वृद्धि: निर्यात को 20 अरब डॉलर से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर करना।
• व्यापार अधिशेष: लगभग 25 अरब डॉलर का शुद्ध व्यापार अधिशेष अर्जित करना।
• वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भागीदारी: भारत की हिस्सेदारी को 3% से बढ़ाकर 8% तक ले जाना।
• रोजगार सृजन: 20 से 25 लाख नए रोजगार पैदा करना, जिससे इस क्षेत्र में कुल प्रत्यक्ष रोजगार 30 से 40 लाख तक हो सके।
निष्कर्ष:
भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र अपार संभावनाओं से भरपूर है, लेकिन इस क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग जगत और नीतिगत संस्थाओं के बीच समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। निर्माण और निर्यात क्षमताओं में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन वैश्विक मूल्य श्रृंखला में और गहराई से जुड़ने की आवश्यकता है ताकि भारत एक वैश्विक ऑटोमोबाइल हब के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके।
तकनीकी परिवर्तन, रणनीतिक नीति समर्थन और कुशल कार्यबल के मेल से भारत अपने वैश्विक स्थान को पुनः परिभाषित कर सकता है। जैसे-जैसे उद्योग पारंपरिक फैक्ट्री मॉडल से स्मार्ट, कनेक्टेड प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है, भारत को इस बदलाव का नेतृत्व करने और वैश्विक ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए तैयार रहना होगा।
| मुख्य प्रश्न: वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की ओर बढ़ रहा है। भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए इस बदलाव से क्या चुनौतियाँ और अवसर उत्पन्न होते हैं? चर्चा करें। |