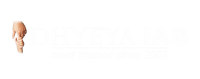संदर्भ –
हिंदी मुख्यधारा का सिनेमा सामाजिक धारणाओं को आकार देने वाला एक शक्तिशाली माध्यम रहा है। हालांकि, यदि इसका आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाए तो पात्रों और कहानियों के चित्रण में एक महत्वपूर्ण असंतुलन दिखाई देता है, बॉलीबुड की ज़्यादातर फिल्में मुख्य रूप से सामाजिक अभिजात वर्ग के जीवन और चिंताओं पर केंद्रित होती हैं। इस लेख मे हम दलित-बहुजन-आदिवासी पात्रों के कम प्रतिनिधित्व और उनके सामाजिक-सांस्कृतिक अनुभवों पर जोर देने वाली फिल्मों के सूक्ष्म पहलुओं पर गौर कर रहे हैं।
मुख्यधारा के सिनेमा और सामाजिक अभिजात वर्ग
हिंदी सिनेमा ने मनोरंजक कहानियों, गीतों, नृत्य और नाटकीय एक्शन दृश्यों के साथ विश्व स्तर पर अपनी जगह बनाई है। जहां बड़े कलाकारो वाली ब्लॉकबस्टर फिल्में बॉक्स-ऑफिस पर सफलता का परचम फहराती हैं, वहीं सामाजिक यथार्थवाद और रचनात्मक सामग्री वाली फिल्में पर्याप्त दर्शकों को खोजने के लिए भी संघर्ष करती हैं। यह लोकप्रिय प्रवृत्ति अक्सर सिनेमा के बौद्धिक और कलात्मक कौशल की गहन परीक्षण में बाधा डालती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे फिल्म उद्योग में सामाजिक अभिजात वर्ग का प्रभुत्व कायम रहता है, जिसके परिणामस्वरूप दलित-बहुजन-आदिवासी पात्रों की फिल्मे उपेक्षा की शिकार हो जाती है। हिन्दी फिल्मों की मुख्य धारा में जाति-संबंधी मुद्दों को छिटपुट रूप से ही चित्रित किया जाता है, इनका प्रतिनिधित्व अक्सर कम किया जाता है और इनको 'गरीब' या 'आम आदमी' जैसी निष्क्रिय श्रेणियों के तहत शामिल किया जाता है। हिन्दी सिनेमा में यह बहिष्कार फिल्म उद्योग और निचली जातियों के पारंपरिक मुद्दों के बीच एक ऐतिहासिक अलगाव को दर्शाता है।
दलित प्रतिनिधित्वः
रूढ़िवादी और अपरिवर्तनीय स्थितियाँ:
हिंदी सिनेमा में जो दलित प्रतिनिधित्व दिखाया गया उसमे अक्सर रूढ़िवादी धारणाओं को कायम रखा गया है, जो उनकी अनिश्चित वर्ग स्थितियों, गरिमा का उल्लंघन और अशिष्ट सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। शायद ही कभी दलित चरित्र सामान्य व्यक्तियों के रूप में उभरे हों जिनके इर्द-गिर्द एक लोकप्रिय कथा घूम सकती हो। इसके बजाय, उन्हें लगातार उनकी जाति पहचान के रूप में चित्रित किया जाता है, जबकि उच्च जाति का नायक लोगों की आकांक्षाओं के प्रतीक की भूमिका निभाता है।
स्वतंत्रता के बाद के सिनेमा में बहिष्करणः
बाबासाहेब अम्बेडकर जैसी हस्तियों के नेतृत्व में सामाजिक न्याय और मुक्ति पर सामाजिक-राजनीतिक चर्चाओं के बावजूद, स्वतंत्रता के बाद के सिनेमा मे दलित मुद्दों के बारे में जागरूकता की कमी दिखाई देती है। अस्पृश्यता को संबोधित करने वाली कुछ फिल्में, जैसे कि बिमल रॉय की सुजाता (1957) ने अंबेडकरवादी दृष्टिकोण के बजाय गांधीवादी समाधान प्रस्तुत किया।
1980 के दशक में समानांतर सिनेमा का उदय हुआ, जिसमे सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, भ्रष्टाचार और जाति-आधारित शोषण को दिखाया गया। इस दौरान निशांत (1975) और दामुल (1985) जैसी फिल्मों ने दलितों की दुर्दशा को प्रामाणिकता के साथ चित्रित किया, लेकिन वे दलित आंदोलन के साथ-साथ दलित संघर्षों और सामाजिक परिवर्तन की उभरती आवाजों को पकड़ने में विफल रहीं।
ब्लॉकबस्टर फिल्मों में बहिष्करणः
'जवान', 'पठान', 'एनिमल', 'गदरः एक प्रेम कथा' और 'ओह माई गॉड' सहित पिछले वर्ष की प्रमुख हिट फिल्मों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उच्च जाति के पात्र मुख्य नायक के रूप में हावी हैं। यह प्रवृत्ति, जब शीर्ष 100 हिंदी सुपरहिट फिल्मों के सर्वेक्षण में देखी गई है, यह दलित-बहुजन-आदिवासी पात्रों के लगातार बहिष्कार को रेखांकित करता है, जो मुख्यधारा के हिंदी सिनेमा को सामाजिक अभिजात वर्ग के हितों और चिंताओं को दर्शाता है।
दलित-बहुजन-आदिवासी पात्रों का सीमित प्रतिनिधित्वः
अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे प्रमुख अभिनेताओं ने अपनी शानदार फिल्मों के बावजूद शायद ही कभी ऐसी भूमिकाएँ निभाई हैं जो प्रामाणिक रूप से दलित-बहुजन-आदिवासी समूहों की चिंताओं और पहचान का प्रतिनिधित्व करती हैं।हालांकि बैंडिट क्वीन (1994) एकलव्य (2007) और आरक्षण (2011) जैसी फिल्मों ने नई दलित पीढ़ी के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों का प्रदर्शन किया है । उदाहरण के लिए, अमिताभ बच्चन द्वारा "एकलव्य" में एक दलित चरित्र का चित्रण एक दुर्लभ अपवाद है। उच्च जाति के नायकों का यह स्पष्ट मूल्यांकन इस धारणा को मजबूत करता है कि दलित-बहुजन-आदिवासी व्यक्ति पर्दे पर औचित्यपूर्ण भूमिकाओं को मूर्त रूप देने में असमर्थ हैं।
अभिजात वर्ग के हितों का चित्रण
फिल्म उद्योग मे लाभ और लोकप्रियता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सामान्य मनोरंजन के लिए फिल्में बनाने की प्रवृत्ति रही है। दुर्भाग्य से, फिल्म निर्माण, प्रदर्शन, वितरण और मनोरंजन व्यवसाय में सामाजिक अभिजात वर्ग के प्रभुत्व ने हिंदी फिल्म उद्योग को एक वर्ग विशेष के प्रतिनिधित्व में बदल दिया है, जो अन्य वर्गों को निष्क्रिय उपभोक्ताओं के रूप में हाशिए पर डाल रहा है। यह अनन्य प्रकृति एक मजबूत पूंजीवादी मॉडल को मजबूत करती है जो कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के हितों को पूरा करता है।
दर्शकों के रूप में दलित-बहुजन-आदिवासी
दलित-बहुजन-आदिवासी दर्शक, जिन्हें अक्सर केवल दर्शकों की भूमिका के लिए छोड़ दिया जाता है, सिनेमाई कथाओं और फिल्म निर्माण के व्यवसाय पर न्यूनतम प्रभाव रखते हैं। ऑन-स्क्रीन नायक, जिन्हें संघर्षरत नायक और सांस्कृतिक एवं नैतिक पहचान के रक्षकों के रूप में चित्रित किया जाता है, एक विषम प्रतिनिधित्व को कायम रखे हुए हैं जो मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम को मजबूत करता है। यह दलित-बहुजन-आदिवासी व्यक्तियों को सिनेमाई क्षेत्र से अलग करता है, जिससे उनके जीवन के अनुभवों और आकांक्षाओं का पता नहीं चलता है।
लोकतंत्रीकरण की आवश्यकताः सिनेमा का लोकतंत्रीकरण करने के लिए, पारंपरिक फिल्म निर्माताओं को दलित-बहुजन-आदिवासी समूहों के मुद्दों और चिंताओं के साथ जुड़ना चाहिए, जिससे उन्हें स्क्रीन पर समान स्थान मिल सके। इसके अतिरिक्त, फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में दलित-बहुजन-आदिवासी पृष्ठभूमि के अधिक तकनीशियनों और कलाकारों को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे विविध दृष्टिकोण और कथाएं सुनिश्चित हों सके, जो सामाजिक वास्तविकताओं के साथ प्रतिध्वनित हों।
दलित-बहुजन सिनेमा की भूमिकाः
पा रंजीत, नागराज मंजुले, मारी सेल्वराज, नीरज घईवान और अन्य फिल्म निर्माताओं के उदय ने सिनेमा की एक नवीन 'दलित शैली' का मार्ग प्रशस्त किया है, विशेष रूप से तमिल और मराठी फिल्म उद्योगों में देखा जा सकता है। ये फिल्म निर्माता शक्तिशाली दलित-बहुजन-आदिवासी पात्रों को प्रस्तुत करते हैं, कहानी कहने की नई तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं और रचनात्मक कथाओं को प्रस्तुत करते हैं जो दर्शकों वर्गो का प्रतिध्वनित करती हैं। दलितों द्वारा निर्देशित और निर्मित मद्रास (2014), सैराट (2016), कर्णन (2021) और झुंड (2022) जैसी फिल्मों के निर्माण के साथ विकासक्रम जारी है। इन फिल्मों में जीवंत दलित नायकों को रूढ़ियों को चुनौती देते हुए और पारंपरिक सिनेमा को बाधित करते हुए दिखाया गया है साथ ही ये नायक हाशिए पर रहने वाले समुदायों को आवाज देकर आलोचनात्मक प्रतिबिंब का ज्यादा प्रदर्शन कर रहे है। हालाँकि, फिल्म उद्योग को लोकतांत्रिक बनाने के लिए दलित-बहुजन सिनेमा शैली की परिवर्तनकारी क्षमता एक दूर की संभावना बनी हुई है।
सिनेमा का लोकतंत्रीकरणः सिनेमा का लोकतंत्रीकरण करने के प्रयासों में न केवल पर्दे पर दलित-बहुजन-आदिवासी समूहों के सामाजिक हितों और राजनीतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करना शामिल है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना शामिल है कि फिल्म उद्योग के लाभ और विशेषाधिकारों को समान रूप से वितरित किया जाए। एक अधिक समावेशी और विविध फिल्म परिदृश्य को बढ़ावा देकर, उद्योग सामाजिक वास्तविकताओं की सूक्ष्म समझ में योगदान कर सकता है और साझा सांस्कृतिक पहचान की भावना को बढ़ावा दे सकता है।
निष्कर्ष
मुख्यधारा के हिंदी सिनेमा के भीतर फिल्म निर्माण में असंतुलन इस उद्योग के गहरे निहित पूर्वाग्रहों और अनन्य प्रथाओं का प्रतिबिंब है। दलित-बहुजन-आदिवासी पात्रों का कम प्रतिनिधित्व न केवल सामाजिक रूढ़ियों को दर्शाता है बल्कि सिनेमा के लोकतंत्रीकरण में भी बाधा डालता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए फिल्म निर्माताओं, उद्योग के हितधारकों और दर्शकों से मौजूदा मानदंडों को चुनौती देने और अधिक समावेशी एवं विविध सिनेमाई परिदृश्य को अपनाने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है।
|
यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न -
|
Source- The Hindu