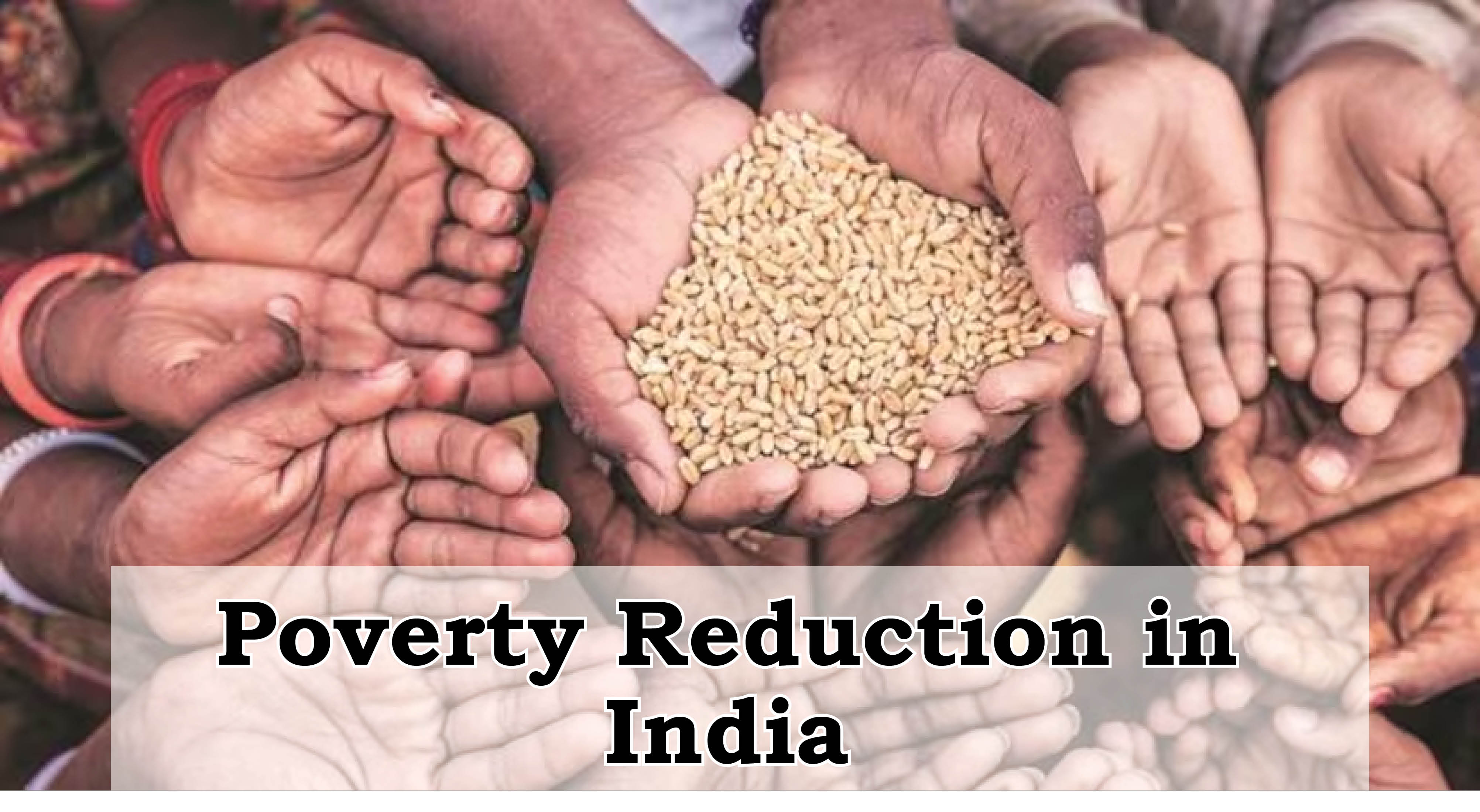परिचय-
गरीबी एक जटिल मुद्दा है, जो सिर्फ आय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि भोजन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आवास तक पहुंच को भी प्रभावित करता है। पिछले एक दशक में भारत ने गरीबी में उल्लेखनीय कमी देखी है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में दिखाई देती है। इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं, जिनमें आर्थिक वृद्धि, सामाजिक कल्याण योजनाएं और गरीबी के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने वाली नीतिगत पहल शामिल हैं।
इन परिवर्तनों का आकलन करने के लिए, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) और बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) जैसे डेटा स्रोत गरीबी में कमी के रुझानों को समझने में मदद करते हैं। ये रिपोर्टें दिखाती हैं कि विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों, साथ ही ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों में गरीबी के स्तर में कैसे बदलाव आए हैं। निष्कर्षों से यह संकेत मिलता है कि विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों के बीच की खाई कम हो रही है, जो व्यापक आर्थिक और सामाजिक विकास को दर्शाता है।
हालांकि गरीबी में कमी एक सकारात्मक विकास है, लेकिन इस प्रगति को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। शिक्षा, रोजगार के अवसर, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा उपायों में सुधार जारी रखना आवश्यक होगा ताकि गरीबी की पुनरावृत्ति को रोका जा सके और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखा जा सके।
घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण को समझना-
महामारी के बाद उपभोग प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 2022-23 और 2023-24 के लिए लगातार दो घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) किए। पहला सर्वेक्षण अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के बीच किया गया था, जिसकी संक्षिप्त रिपोर्ट फरवरी 2024 में और विस्तृत रिपोर्ट जून 2024 में जारी की गई। दूसरा सर्वेक्षण, जो अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक चला, हाल ही में प्रकाशित किया गया।
घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, घरेलू खर्च के पैटर्न पर डेटा एकत्र करता है ताकि आर्थिक कल्याण का आकलन किया जा सके, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को अपडेट किया जा सके और गरीबी व असमानता को मापा जा सके। 2023-24 के सर्वेक्षण में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 2,61,953 घरों को शामिल किया गया।
गरीबी के रुझानों का आकलन करने के लिए, अध्ययन में सी. रंगराजन विशेषज्ञ समूह द्वारा 2014 में सुझाई गई गरीबी रेखा का उपयोग किया गया, हालांकि इसे भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से नहीं अपनाया था। यह गरीबी रेखा निम्नलिखित आधारों पर तय की गई है:
1. संशोधित मिश्रित पुनः स्मरण अवधि (MMRP): घरेलू खर्च डेटा संग्रह की एक विस्तृत विधि, जिसे विशेषज्ञ अधिक सटीक मानते हैं।
2. पोषण मानक: खाद्य घटक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा निर्धारित कैलोरी सेवन आवश्यकताओं पर आधारित है।
3. गैर-खाद्य घटक: शिक्षा, आवास, ईंधन, कपड़े और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक जरूरतों को शहरी क्षेत्रों में अधिक महत्व दिया गया।
2023-24 के लिए, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश (UT) की गरीबी रेखाओं को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर अपडेट किया गया। इस विश्लेषण में 2011-12 में 1 लाख से अधिक घरों और 2023-24 में 2.5 लाख घरों के लिए किए गए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि सर्वेक्षण डेटा का उपयोग किया गया।

समग्र गरीबी में कमी के रुझान (2011-12 से 2023-24)-
निष्कर्षों से पता चलता है कि पिछले 12 वर्षों में भारत में गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट आई है:
- ग्रामीण गरीबी 30.4% से घटकर 3.9% हो गई।
- शहरी गरीबी 26.4% से घटकर 3.9% हो गई।
धार्मिक समूहों में गरीबी में कमी-
गरीबी में सभी धार्मिक समुदायों में गिरावट देखी गई, विशेष रूप से हिंदू और मुस्लिम समुदायों में:
ग्रामीण क्षेत्र:
- 2011-12 में, मुस्लिम गरीबी दर 31.7% थी, जो हिंदू गरीबी दर (30.9%) से 0.8 प्रतिशत अंक अधिक थी।
- 2023-24 तक, मुस्लिम गरीबी 2.4% और हिंदू गरीबी 4% हो गई, जिससे अंतर -1.6 प्रतिशत अंक हो गया।
शहरी क्षेत्र:
- 2011-12 में, मुस्लिम गरीबी 39.4% थी, जो हिंदू गरीबी (24.4%) से 15 प्रतिशत अंक अधिक थी।
- 2023-24 तक, मुस्लिम गरीबी 5.7% और हिंदू गरीबी 3.7% हो गई, जिससे अंतर केवल 2 प्रतिशत अंक रह गया।
मुस्लिम समुदाय में गरीबी में गिरावट (33.7 प्रतिशत अंक) हिंदू समुदाय (20.7 प्रतिशत अंक) की तुलना में अधिक तेज़ रही, जो इस समुदाय में तेजी से आर्थिक सुधार को दर्शाता है।
सामाजिक समूहों में गरीबी में कमी-
ग्रामीण क्षेत्र:
• अनुसूचित जनजाति (एसटी): गरीबी 2011-12 में 49.5% से घटकर 2023-24 में 12.2% हो गई। एसटी-सामान्य श्रेणी का गरीबी अंतर 29.5 प्रतिशत अंक से घटकर 10.6 प्रतिशत अंक रह गया।
• अनुसूचित जाति (एससी): गरीबी 45.5% से घटकर 8.6% हो गई, जिससे एससी-सामान्य गरीबी अंतर 17.4 प्रतिशत अंक से घटकर 2.6 प्रतिशत अंक रह गया।
• अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी): गरीबी 30.4% से घटकर 3.6% हो गई।
शहरी क्षेत्र:
• एससी जनसंख्या: गरीबी 39.6% से घटकर 6.6% हो गई (33 प्रतिशत अंकों की गिरावट)। एससी-सामान्य गरीबी अंतर 20 प्रतिशत अंक से कम होकर 4.1 प्रतिशत अंक हो गया।
• एसटी जनसंख्या: गरीबी 38.2% से घटकर 9.9% हो गई, एसटी-सामान्य श्रेणी का अंतर 21.5 प्रतिशत अंक से घटकर 7.4 प्रतिशत अंक हो गया।
• ओबीसी जनसंख्या: गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई, जो 30.4% से घटकर 3.6% हो गई।
प्रमुख निष्कर्ष और नीतिगत प्रभाव-
1. व्यापक गरीबी में कमी: सभी धार्मिक और सामाजिक समूहों में गरीबी की समग्र गिरावट आर्थिक वृद्धि और सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता को दर्शाती है।
2. वंचित समुदायों के लिए महत्वपूर्ण सुधार: मुस्लिम, SC और ST समुदायों में सबसे अधिक लाभ देखा गया, जिससे ऐतिहासिक असमानताएं कम हुईं।
3. समूहों के बीच सामंजस्य: गरीबी अंतर कम होने से आर्थिक समानता में वृद्धि का संकेत मिलता है।
4. सरकारी नीतियों का प्रभाव: विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम इस प्रगति में महत्वपूर्ण रहे।
सतत प्रगति के लिए रणनीतियाँ-
1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण: बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन कवरेज का विस्तार करें, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए 100% स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और सामाजिक सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें।
2. रोजगार और आजीविका: मनरेगा के तहत रोजगार सृजन को मजबूत करना, जिला कौशल केंद्रों के माध्यम से कौशल मानचित्रण करना और लक्षित प्रशिक्षण प्रदान करना।
3. महिला सशक्तिकरण: निर्णय लेने और आर्थिक गतिविधियों में महिला भागीदारी को बढ़ाना।
4. बुनियादी ढाँचा विकास: आर्थिक गतिशीलता और सेवा पहुँच को बढ़ावा देने के लिए सड़कों, स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में सुधार करना।
5. डिजिटल और वित्तीय समावेशन: सरकारी योजनाओं तक वास्तविक समय की पहुँच के लिए eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाज़ार) जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर किसानों का पूर्ण डिजिटल पंजीकरण सुनिश्चित करना।
6. आपदा तैयारी और जलवायु कार्रवाई: आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना करना और कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) के माध्यम से जलवायु-लचीली कृषि को बढ़ावा देना।
निष्कर्ष
पिछले दशक में भारत ने गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, विशेष रूप से वंचित समुदायों के बीच। यह प्रगति आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण योजनाओं और नीतिगत सुधारों का परिणाम है, जिनका उद्देश्य जीवन स्तर में सुधार करना रहा है। हालांकि, इन उपलब्धियों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इन निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र केवल चुनाव संपन्न कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य लोगों के जीवन में ठोस सुधार लाना है। सुशासन का दायित्व है कि वह ऐसी नीतियों को प्राथमिकता दे जो समान अवसरों को बढ़ावा दें और समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से सबसे कमजोर तबकों के उत्थान पर केंद्रित हों।
| मुख्य प्रश्न: भारत में गरीबी के रुझान को मापने में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) की भूमिका का मूल्यांकन करें। HCES के डेटा ने गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से नीतिगत निर्णयों को कैसे संबोधित किया है? |